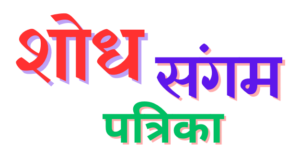| 1 |
Author(s):
गरिमा सिंह.
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
1-8 |
असगर वजाहत के नाटकों में सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप
Abstract
भारतीय संस्कृति एक सामासिक संस्कृति रही है। इसके निर्माण में बहुत लंबा समय लगा है इस कारण इसका मिलाजुला रूप दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि विभिन्न धर्म. जाति के लोग रहने पर भी इनर्क परम्परा. संस्कार. रीति-रिवाज. त्यौहार. भाषा अलग-अलग होने पर भी भारत संस्कति में एक समरूपता दिखाई देती है। असगर वजाहत एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया है। इनके नाटक हिन्दू- मुस्लिम एकता की मिसाल प्रस्तुत करते हैं और भारतीय सांस्कृतिक चेतना को और भी मजबूत बनाने में सराहनीय योगदान देते हैं।
| 2 |
Author(s):
सुनील सिंह पंवार.
Research Area:
शिक्षा शास्त्र
Page No:
9-15 |
भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव
Abstract
भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव एक महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है। यह शोध पत्र भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे योग, आयुर्वेद, भारतीय धर्म, कला, और साहित्य के माध्यम से पूरे विश्व में फैलने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। भारतीय संस्कृति ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि दुनिया भर के देशों और संस्कृतियों को भी प्रभावित किया है। योग और आयुर्वेद जैसे भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ अब विश्वभर में लोकप्रिय हो चुकी हैं। भारतीय कला, साहित्य, और दर्शन ने भी अन्य देशों के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह शोध पत्र यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और इसके तत्व वैश्विक स्तर पर मानवता, शांति, और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं।
| 3 |
Author(s):
Ravi Verma.
Research Area:
भूगोल
Page No:
16-21 |
भारत में ऊर्जा संकट: कारण और समाधान
Abstract
भारत में ऊर्जा संकट एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र को प्रभावित कर रही है। इसका मुख्य कारण ऊर्जा संसाधनों की कमी, बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा की मांग, और ऊर्जा वितरण की असमानताएँ हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक स्रोतों की समाप्ति और अक्षय ऊर्जा के अपर्याप्त विकास ने इस संकट को बढ़ाया है। साथ ही, ऊर्जा संकट का सामाजिक प्रभाव भी गहरा है, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी और जीवनस्तर पर असर पड़ता है। समाधान के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा के अधिकतम उपयोग, ऊर्जा दक्षता सुधार, और वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके अलावा, सरकार की नीति और योजनाओं में सुधार और ऊर्जा संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन भी ऊर्जा संकट के समाधान के लिए जरूरी है। इस शोध पत्र का उद्देश्य ऊर्जा संकट की जटिलताओं को समझते हुए इसके स्थायी और प्रभावी समाधान प्रदान करना है, ताकि भारत में ऊर्जा की उपलब्धता और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
| 4 |
Author(s):
रचना सिंह.
Research Area:
शिक्षा शास्त्र
Page No:
22-27 |
स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली: समस्याएँ और समाधान
Abstract
भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली व्यापक और विविध है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इस प्रणाली में कई समस्याएँ हैं, जैसे- स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, गुणवत्ता में अंतर, और चिकित्सा भ्रष्टाचार। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बड़ी चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियों के कारण कई लोग गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं। समाधान के तौर पर, सरकार को स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करनी चाहिए और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विस्तार करना चाहिए। इसके साथ ही, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, और प्रौद्योगिकी का उपयोग (जैसे टेलीमेडिसिन) स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। निजी क्षेत्र की निगरानी और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
| 5 |
Author(s):
नीलम संजीव एक्का.
Research Area:
समाजशास्त्र
Page No:
28-34 |
छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में विद्यमान जैव विविधता संरक्षण की परंपरा
Abstract
सारांश- जनजातीय संस्कृति द्वारा जैव विविधता संरक्षण वैश्विक पटल पर अनूठा एवं महत्वपूर्ण विषय है,जो पारंपरिक ज्ञान,सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ है| जनजातीय समुदायों का जीवन न केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़ा हुआ हैबल्कि यह जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| यह शोधपत्र जनजातीय समुदायों की संस्कृति,उनके पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता के संरक्षण की विधियों पर केन्द्रित है| प्रस्तुत शोधपत्र द्वारा यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आधुनिक विकास,औद्योगिकीकरण और पर्यावरणीय बदलाव इन समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं |
| 6 |
Author(s):
Archana kushawaha .
Research Area:
राजनीति विज्ञान
Page No:
35-39 |
शिक्षा का अधिकार और समाज में जागरूकता
Abstract
शिक्षा किसी भी राष्ट्र के प्राणतत्व की तरह होती है। शिक्षा के माध्यम से ही कोई भी राष्ट्र सभ्य बनकर उन्नति के मार्ग पर खुद को प्रशस्त करता है। किंतु भारतीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता अन्य देशों की तुलना में कम देखने को मिलता है। प्रस्तुत शोध शिक्षा का अधिकार एवं समाज में जागरूकता विषय पर चर्चा करते हुए, शिक्षा के प्रति कम जागरूकता के कारणो का अध्ययन करते हुए संभावित उपायों को प्रस्तुत करती है।
| 7 |
Author(s):
Madhavi Abichandani, Dr.S K. Thakur.
Research Area:
वाणिज्य
Page No:
40-48 |
महिला सशक्तिकरण
Abstract
सार- बदलती परिस्थितियों के साथ आज 21 वीं सदी में महिलाओं को सषक्त व सबल बनाने के प्रयासों का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। आज की नारी किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है। वैदिक काल से वर्तमान तक अनेक उतार-चढ़ाव देखते हुए, समाज सुधारकों के अथक प्रयासों, वर्षों से सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के परिणाम स्वरुप एवं स्वयं के असीम संघर्षों के पष्चात् भारतीय नारी शताब्दियों की परतंत्रता की बेडियों के बंधन से मुक्त हुई, उसने सार्वजनिक जीवन में प्रवेष किया, जिससे वह पति सेवा के अतिरिक्त राष्ट्र जाति एवं स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझ सकी। अपने अधिकारों के प्रति उसमें जागरुकता पैदा हुई, उसने घर की चारदीवारी को लांघकर, परम्परागत सीमाओं को तोड,़ समाज में अपने महत्वपूर्ण योगदान द्वारा नवीनता को प्रतिस्थापित किया। महिलाओं में अपने पैरों पर खडे होने का स्वावलम्बन प्रस्फुटित होने लगा व उसने स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया। षिक्षा और आर्थिक मजबूती ने नारी आत्मविष्वास में वृद्धि की। आज की नारी पुरुष वर्चस्व अधिकार क्षेत्र की प्राचीरों को तोड़ने में प्रयासरत है। वह स्वेच्छानुसार अपने व्यक्तित्व निर्माण की दिषा में शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रषासनिक एवं खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नये आयाम तय कर रही है। आर्थिक दृष्टि से आज की नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है ।
| 8 |
Author(s):
श्री हेमेन्द्र कुमार, डॉ. बीरेंद्र कुमार शर्मा.
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
49-53 |
मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का संक्षिप्त अध्ययन
Abstract
समकालीन हिन्दी उपन्यासकारों में मैत्रेयी पुष्पा का नाम अग्रगण्य रहा है | इन्होनें अपनी रचनाओं के द्वारा हिन्दी साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है | इनके उपन्यासों में नारीवाद जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के रूप में प्रस्फुटित हुआ है | नारी के दु:ख-दर्द, संताप, पीड़ा, संवेदना, नारी शोषण, रूढ़ व्यवस्था की दास्तान अपने उपन्यासों में व्यक्त की है | इनके उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय निम्नांकित है |
| 9 |
Author(s):
चमन लाल.
Research Area:
संस्कृत
Page No:
54-58 |
षोडश संस्कार की वैज्ञानिकता एवं ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व: गर्भाधान संस्कार
Abstract
हमारे ऋषिमुनियों द्वारा स्थापित षोड्श संस्कार में गर्भाधान संस्कार पहले स्थान पर आता है। गर्भाधान संस्कार के द्वारा किसी भी जातक का भविष्य तय होता है। ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र में गर्भाधान करने की मुहूर्त एवं विधि बतायी गई हैं। किस समय गर्भाधान संस्कार करने से गर्भधारण होगा? किस मुहूर्त में गर्भाधान करने से पुरुष जातक उत्पन्न होंगे किस मुहूर्त में स्त्री जातक उत्पन्न होगी? यदि गर्भधारण न हो रही हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। अधुना लोग गर्भाधान तो करते परन्तु गर्भधान संबंधी संस्कार नहीं करते। इस लेख के द्वारा गर्भाधान की वैज्ञानिकता एवं ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व के बारे में बताया गया है।
| 10 |
Author(s):
डॉ मीना सेंगर.
Research Area:
राजनीति विज्ञान
Page No:
59-62 |
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओ के संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन
Abstract
भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इन समुदायों की महिलाओं को जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान ने इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिनमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 39, 46 और 243क् शामिल हैं। यह शोध पत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का विश्लेषण करता है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए कानूनी प्रयासों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, यह पत्र इन अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है।
| 11 |
Author(s):
KRISHNA KUMAR SARHAN.
Research Area:
शिक्षा शास्त्र
Page No:
63-73 |
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षकों की धारणाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
Abstract
स्कूली शिक्षा समाज के बौद्धिक और नैतिक विकास की नींव रखती है। इसकी गुणवत्ता केवल पाठ्यक्रम की संरचना या परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं होती, बल्कि शिक्षकों की भूमिका, शिक्षण विधियों, विद्यालयी वातावरण, प्रशासनिक सहयोग और संसाधनों की उपलब्धता सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षकों का दृष्टिकोण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शिक्षा प्रणाली के मूल घटक हैं और शैक्षिक सुधारों के प्रभाव को सीधे अनुभव करते हैं। शिक्षकों का मानना है कि पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, कक्षा में संवादात्मक शिक्षण, मूल्यांकन की निष्पक्षता, छात्र-शिक्षक अनुपात, शैक्षिक नवाचारों का समावेश और प्रशासनिक सहयोग, शिक्षा की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताएँ, पेशेवर विकास के अवसर और शिक्षण में तकनीकी संसाधनों का प्रभाव भी इस अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में शामिल हैं। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि विद्यालयी वातावरण और नीति-निर्माण में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार किया जा सकता है। शिक्षकों ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और आधुनिक बनाने के लिए नीतिगत बदलाव आवश्यक हैं। यह शोध नीति-निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिससे एक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण संभव हो सके।
| 12 |
Author(s):
Dr. Arnnada Shankar Acharya.
Research Area:
संस्कृत
Page No:
74-82 |
पुराणे प्रकृति वृक्षमिति जीवनस्य आधार
Abstract
धरित्री मध्ये जीवन सञ्चरणात् पूर्वं तरुणाम् जन्म अभवत् । सम्पुर्ण ब्रह्माण्डस्य मुल्यवान पदार्थमध्यात् वृक्षमिति सर्वोपरि भवति । व्रह्माण्ड मध्ये वहव ग्रहा नक्षत्राञ्च सन्ति तेषां मध्यात् सम्यक् केचनमात्र ग्रहा वासोपोयोगी वर्तते । पृथिवीवत् सर्वे स्वर्णिम मण्डलं मध्ये न सन्ति तथा च न हि तत्र अन्य जीवनं सञ्चारणं प्रमाणमपि वर्तते । पृथिवी एकस्मिन् दुर्लभ निवास स्थान भवति यत्र जीवनस्य सञ्चरण तथा वासोपयोगी अनुकुल पर्यावरणं वर्तते । अत्र प्रत्येक जीव परस्पर चतुर्पार्श्वे आदिम कालात् सुखेन परिवर्धते । विज्ञान मते पुराकाले डाइनोसर् नामक जीव पृथिवीपृष्ठे अभवत् । यदा तस्य सामुहिक जीवनम् एक उल्कापिण्ड माध्यमेन विनाशं भवति तदा स्तन्यपायी प्राणीनां अभ्युदयं वर्तते । तत्पर आदि युगात् अद्यावधि पर्यन्त विश्वस्य श्रेष्ठ जीवरुपे मनुष्यमिति परिचयं लभ्यते । वहव सभ्यता युगानि च व्यतितानि वर्तन्ते किन्तु मानवा इतिहासात् सम्यगमपि शिक्षा न प्राप्नुवन्त । सिन्धु सभ्यतायां प्रत्यक्ष अनुभुत्या परं सम्प्रति मानवा विज्ञानस्य जययात्रा विकासस्य चरम उत्कर्षता लभ्यते तथा स्वस्वार्थं निमित्त वन्य , पशु , परिवेश इत्यादय ध्वसं लीला कृत्वा विकाश पथे अग्रसरति । पुराकाले जनाः प्रकृत्या उपरि निर्भर कृत्वा स्वजीवनम् निर्वाहं अकरोत् । सिन्धु सभ्यतायां अधपतन परं जीवनस्य अभिवृद्धि निमित्त अन्य एक सनन्द मनुष्याणां प्राप्नुवन्त । अभिनव कारीगरी कौशलं माध्यमेन योजनावद्ध्वा मनुष्य स्वनिमित्त वासगृह , सुन्दर प्रासाद , जलं निष्कासनं निमित्त जलनिष्कासनं मार्ग यत् सर्वं नद्या मध्ये प्रविष्टवन्त ।
तत् परं मनुष्याणा वन्धनम् चिन्ता भवति । इत्यस्मिन् अवसरे परिवार मध्ये जन्म , विवाह तथा अन्य आकर्षणिय जीवनशैल्या मध्ये निमग्ना मनुष्या आनन्द सागरे मोहयित्या प्रकृत्या विनाशं आरम्भ्यन्ते । वृक्षाणां विनाशं कृत्वा शान्त स्निग्ध वातावरणयो असन्तुलितवन्त तथा स्व विनाश निमित्तं मार्गं प्रस्तरिर्यते यत् सुनामि , असमये घुर्णिवलय , चक्रवात , वात्या , वन्या , वैशिक तापमात्रा वृद्धि इत्यादयस्य मुल कारणं भवति । वृक्ष इति जीवनस्य मुल आधारशिला वर्तते । यदा वृक्षं न वर्त्तते तदा जीवनम् अपि न भवति ।
| 13 |
Author(s):
Praween Verma.
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
83-89 |
धर्मवीर भारती के साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति
Abstract
धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के उन विशिष्ट रचनाकारों में से हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को गहनता और सूक्ष्मता से व्यक्त किया। यह शोध पत्र उनके साहित्य में प्रेम, दुख, संघर्ष और सामाजिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का विश्लेषण करता है। उनकी प्रमुख रचनाएँ जैसे गुनाहों का देवता, अंधा युग और सूरज का सातवाँ घोड़ा इस अध्ययन का आधार हैं। इन रचनाओं में भारती ने मानव मन की जटिल भावनाओं को पात्रों, कथानक और प्रतीकों के माध्यम से उजागर किया है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि भारती ने व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों में संवेदनाओं को कैसे चित्रित किया और उनकी शैली अन्य समकालीन लेखकों से किस प्रकार भिन्न है। विश्लेषण से पता चलता है कि उनकी रचनाएँ प्रेम और त्याग की कोमलता से लेकर युद्ध और नैतिकता के कठोर प्रश्नों तक संवेदनाओं का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती हैं। यह अध्ययन न केवल भारती के साहित्यिक योगदान को रेखांकित करता है, बल्कि आधुनिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को भी उजागर करता है। निष्कर्षतः, भारती का साहित्य मानवीय संवेदनाओं का एक सशक्त दस्तावेज है, जो पाठकों को आत्म-चिंतन के लिए प्रेरित करता है।
| 14 |
Author(s):
श्री कौशिक राय.
Research Area:
संस्कृत
Page No:
90-94 |
ऋग्वेदस्य सन्दर्भे सोमस्य अधिभूतरूपकचिन्तनम्
Abstract
वैदिकऋषिणां आत्मचिन्तनं त्रिषु बिन्दुषु अवगन्तुं शक्यते । प्रथमं - भौतिकस्तरात् उपरि उत्थाय आध्यात्मिकस्तरं प्राप्तुं स्थूलतः सूक्ष्मपर्यन्तं गन्तुं प्रयत्नः। एकं विश्वजनीनसत्यं, एकं शाश्वतं शक्तिं, अन्य: च अस्य विशालस्य जगतः मूलं एकमेव सर्वव्यापीं बलं च अन्वेष्टुं वैदिकऋषयः प्रयतन्ते इव दृश्यन्ते । वैदिकसंहितातः उपनिषदपर्यन्तं तस्य आविष्कारस्य प्रमाणीकरणानि व्यञ्जनानि प्राप्नुमः। वैदिकऋषिवचने - "सोमं पिबन्तः अमरः अभवाम, दिव्यं प्रकाशं प्राप्तवन्तः, दिव्यानि तत्त्वानि अवगच्छामः" इति। पीतं सोमं किम्? सोमः दिव्यानन्दस्य अमृतम्। तस्य अमृतस्य पिबनेन अमरः भवति नरः। अथ दिव्यं ज्योतिं पश्यति। दिव्यप्रकाशात् सत्यं ज्ञानं प्राप्यते। सोमः वेदानाम् अत्यन्तं गूढं माधुर्यपूर्णं च प्रहेलिका अस्ति| आनन्दस्य आनन्दस्य च अमृतम् इति कथ्यते - आनन्दस्य मधु - मद्यं | महतीं सृजनशीलतां गहनं रहस्यमयदृष्टिञ्च प्रेरयति | जिह्वां गीतं प्रति चालयति . तया वैदिकद्रष्टारः सोमप्रेरितानां गूढश्लोकनिर्गमने एतावन्तः सृजनात्मकाः प्रचुराः च अभवन् सोमः मानवस्य आयुः दीर्घं करोति इति अपि कथ्यते |. अमृतस्य अमृतम् अस्ति - शाश्वतयौवनस्य कथानकस्रोतः| सोमस्य अग्निविस्फोटाः युद्धक्षेत्रेषु योद्धानां अविश्वसनीयं साहसं वीरतां च ददति| ते सर्वं मृत्युभयं , दुःखं च हरन्ति| अतः सोमस्य अस्मिन् एकीकृतरूपेण तस्य अवधारणा उत्पत्तिं तस्य समग्रसन्दर्भस्य च समीक्षां कर्तुं ऋग्वेदपाठपरिक्रमे एषः शिर्षक: विषयः आलोचित: |
| 15 |
Author(s):
Brajesh Kumar Rai, Dr. Anand Kumar Tripathi.
Research Area:
इतिहास
Page No:
95-101 |
1917 से 1942 तक बिहार के किसानों के संघर्षों में राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष
Abstract
1917 से 1942 तक बिहार के किसानों के संघर्षों में राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का अध्ययन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह अवधि भारतीय राजनीति में बदलाव का दौर था, जहां ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आम जनता, खासकर किसानों, ने सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन किया। बिहार, जो कृषि प्रधान राज्य था, यहां के किसानों की समस्याओं और उनके संघर्षों को राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संबोधित किया गया। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलनों ने न केवल बिहार के किसानों को जागरूक किया, बल्कि उन्हें संगठित भी किया। यह समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसान वर्ग की भागीदारी का प्रमुख समय था, और राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। किसानों की मुख्य समस्याएं भूमि कर, जमींदारी प्रथा, और बकाया कर थे, जिनके कारण उनका जीवन अत्यधिक कठिन हो गया था। ब्रिटिश शासन द्वारा निर्धारित ऊंचे कर और अन्य प्रशासनिक नीतियों ने किसानों को शोषण का शिकार बना दिया था। इन समस्याओं का समाधान नहीं होने पर, बिहार के किसान आंदोलनों का हिस्सा बन गए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख बन गए। कांग्रेस ने इन संघर्षों को एक राजनीतिक मंच पर उठाया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्हें सांविधानिक और कानूनी तरीकों से हल करने की दिशा में काम किया।
| 16 |
Author(s):
पूजा कुमारी गुप्ता.
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
102-107 |
अनामिका की काव्य भाषा : स्त्री भाषा के संदर्भ में
Abstract
अनामिका की काव्य भाषा में सहजता, सरलता, प्रवाह मयता का उल्लेख सहज ही मिल जाता है। उनकी काव्य भाषा का लचीलापन उनकी कविताओं में बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है। वह अपनी कविता में लयबद्धता, बिंब, प्रतीक, तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों के माध्यम से काव्य भाषा को समृद्ध किया है। अनामिका की कविता में बदलते परिवेश, टूटते मूल्य और विखंडित होते संयुक्त परिवार, अकेलेपन का संत्रास, स्त्री - पुरुष संबंध में आयी शिथिलता को लेखिका ने अपनी कविता में बखूबी चित्रण किया है। अनामिका की कविता के कैनवास के केंद्र में स्त्री अपने अनेक रूप और रंग में विद्यमान है। महानगर और जनपद, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी बालक और वृद्ध, परिवार और समाज तक उसकी संवेदना का विस्तार है। उपेक्षित मानवीयता और उसकी विवशता भी उनकी कविताओं में प्रकट होती है।